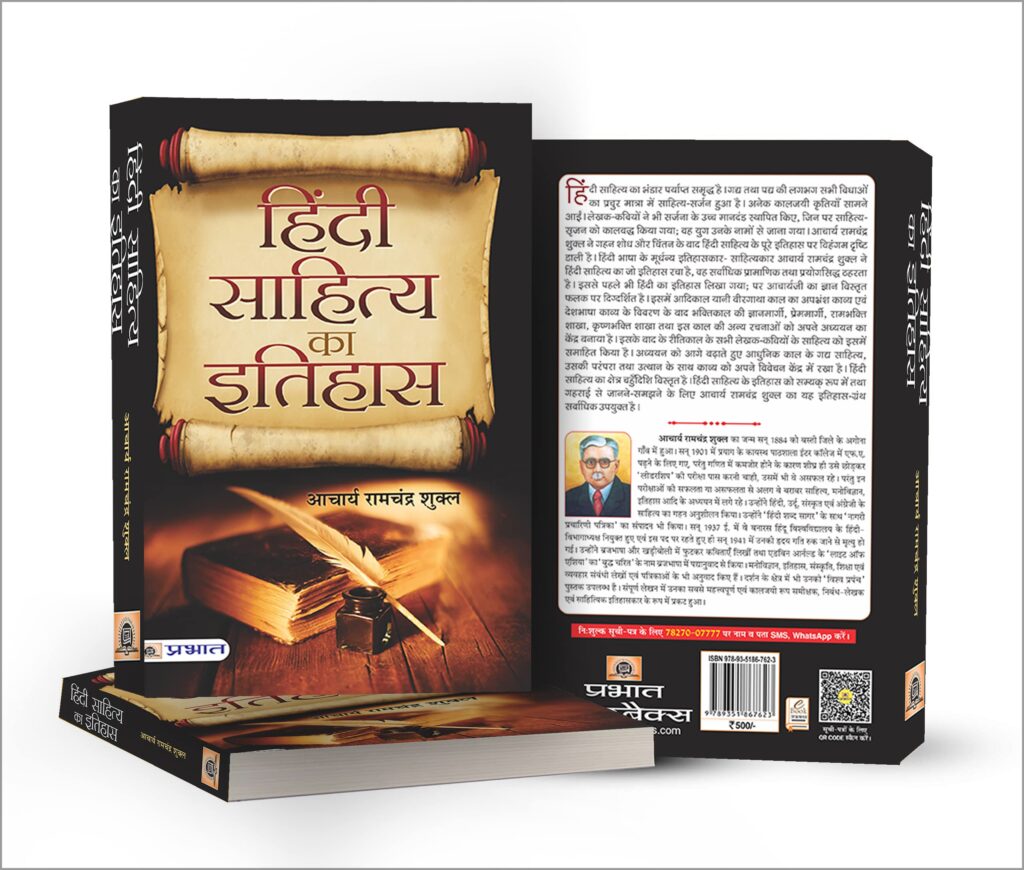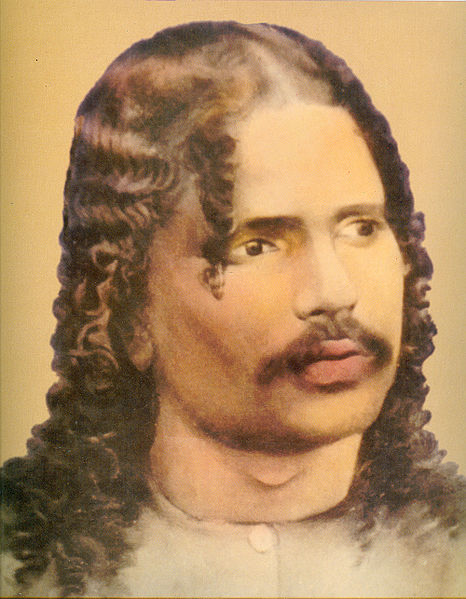आदिकाल : प्रकरण-1
- प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी-साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है ।
- उस समय जैसे “गाथा” कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही “दोहा” या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्यभाषा का पद्य समझा जाता था ।
- अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सब से पुराना पता तांत्रिक और योगमार्ग बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की सातवीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है।
- मुंज और भोज के समय ( संवत् 1050 के लगभग ) में तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य-रचनाओं में भी पाया जाता है।
- अतः हिंदी-साहित्य का आदिकाल संवत् 1050 से लेकर संवत् 1375 तक अर्थात् महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है।
- यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत् 770 में भोज के पूर्वपुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार-ग्रंथ लिखना बताती है (दे० शिवसिंहसरोज ) पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।
- आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम डेढ़ सौ वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है—धर्म, नीति, शृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएँ दोहों में मिलती हैं।
- इस अनिर्दिष्ट लोक-प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है तब से हम हिंदी-साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बँधती हुई पाते हैं।
- राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, शृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों, या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे।
- यही प्रबंध-परपरा ‘रासो’ के नाम से पाई जाती है जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने ‘वीरगाथा-काल’ कहा है।
- दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है।
- असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त हैं उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात् प्राकृताभास (प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध) हिंदी है।
- इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएँ मिलती हैं। वह उस समय के कवियों की भाषा है।
- कवियों ने काव्य-परम्परा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं (जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे), विभक्तियों, कारकचिह्न और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं।
- बोलचाल की भाषा घिस-घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा को बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे कई सौ वर्ष पहले से कवि-परंपरा रखती चली आती थी।
- अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते है, वे उस काव्यभाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदि काल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक—पोथियों में चलती रही।
- विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के मध्य में एक ओर तो पुरानी परंपरा के कोई कवि—संभवतः शार्ङ्गधरि—हम्मीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे—
- चलिअ वीर हम्मीर पाअभर मेइणि कंपइ।
- दिगमग णह अंधार धूलि सुररह आच्छाइहि।।
- दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकरियाँ कह रहे थे—
- एक नार ने अचरज किया। साँप मार पिंजरे में दिया।।
- इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक ओर तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्यभाषा भी भनते रहे—
- बालचंद बिज्जावइ भासा। दुहु नहिं लग्गइ दुज्जन-हासा॥
- और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे—
- अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारि।
- उतर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारि बिचारि॥
- सारांश यह कि अपभ्रंश की यह परंपरा, विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है—पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देशी भाषा का।
- इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है—
- देसिल बसना सब जन मिट्ठा। तें तैसन जंपओं अवहट्ठा॥
- अर्थात् देशी भाषा (बोलचाल की भाषा) सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश (देशी भाषा मिला हुआ) मैं कहता हूँ।
- विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न, प्रचलित बोलचाल की भाषा को “देशी भाषा” कहा है। अतः हम भी इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकतानुसार करेंगे।
- इस आदि काल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देशभाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे।
प्रकरण-2 : अपभ्रंश काव्य
- जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश-साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए।
- पहले जैसे ‘गाथा’ या ‘गाहा’ कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही पीछे “दोहा’ या ‘दूहा’ कहने से अपभ्रंश या लोकप्रचलित काव्यभाषा का बोध होने लगा।
- इस पुरानी प्रचलित काव्यभाषा मे नीति, शृंगार, वीर आदि की कविताएँ तो चली ही आती थी, जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिये भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे।
- प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य-रचना के लिये रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला।
- जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक-वह भाषा या देशभाषा ही कहलाती रही, जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिये अपभ्रश शब्द का व्यवहार होने लगा।
- भरत मुनि (विक्रम तीसरी शती) ने ‘अपभ्रंश’ नाम न देकर लोकभाषा को ‘देशभाषा’ ही कहा है।
- वररुचि के ‘प्राकृत प्रकाश’ में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है ।
- ‘अपभ्रंश’ नाम पहले पहल बलभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिससे उसने अपने पिता गुहसैन ( वि० सं० 650 के पहले ) को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है।
- भामह (विक्रम 9 वीं शती ) ने भी तीनों भाषा का उल्लेख किया है।
- बाण ने ‘हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषाकवियों का भी उल्लेख किया है ।
- इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमे विक्रम की सातवीं शताब्दी से मिलता है।
- उस काल की रचना के नमूने बौद्धो की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिले है।
- संवत् 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं। उन्होने भी ‘श्रावकाचार’ नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंस का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए हैं, जैसे-
जो जिण सासण भाषियउ सो मई कहियउ सारु।
जो पालम सइ भाउ करि सो तरि पावई पारु।
- इन्हीं देवसेन ने ‘दब्ब-सहाव-पयास’ (द्रव्य-स्वभाव-प्रकाश) नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल्ल धवल ने ‘गाथा’ या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया।
- इसके पीछे तो जैन कवियो की बहुत सी रचनाएँ मिलती हैं, जैसे श्रुतिपंचमी कथा, योगसार, जसहरचरिउ, णयकुमारचरिउ इत्यादि।
- ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र-काव्य या आख्यानकाव्य के लिये अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है।
- पुष्पदंत ( संवत् 1029) के ‘आदिपुराण’ और उत्तर पुराण’ चौपाइयों में हैं।
- उसी काल के आस-पास का असहचरिउ” (यशधर-चरित्र) भी चौपाइयों में रचा गया है, जैसे-
विणु धवलेण सयडु किं हल्लई । बिणु जीवेण देहु किं चल्लइ।
विणु जीवेण मोख्य को पावइ । तुम्हारसु किं अप्पइ आवइ।।
- चौपाई-दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों मे, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्रप्रकाश, व्रजविलास, सबलसिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान-काव्यों में पाते हैं।
- बौद्धधर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूरबी भागो में बहुत दिनों से चला आ रहा था।
- इन बौद्ध तान्त्रिको के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुँचा।
- ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे!
- चौरासी सिद्ध इन्हीं में हुए हैं जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तात्रिक योगियों को लोग अलौकिक-शक्ति-संपन्न समझते थे।
- ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिये प्रसिद्ध थे- राजशेखर ने ‘कर्पूरमंजरी’ में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है।
- इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शती से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा
- बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे।
- बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब ये तितर-बितर हो गए। बहुत से भोट आदि देशों को चले गए।
- सिद्धों की संख्या चौरासी है।
- सिद्धों के नाम में ‘पा’ आदरार्थक ‘पाद’ शब्द है। इस सूची के नाम पूर्वापर कालानुक्रम से नही है। इनमें से कई एक समसामयिक थे।
- वज्रयान शाखा में जो योगी ‘सिद्ध’ के नाम से प्रसिद्ध हुए वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे।
- इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी बानी अपभ्रंश-मिश्रित देशभाषा या काव्यभाषा में भी बराबर सुनाते रहे।
- उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले म॰ म॰ हरप्रसाद शास्त्री ने बँगला अक्षरों में “बौद्धगान ओ दोहा” के नाम से निकाला था।
- पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायनजी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएँ लाए।
- सिद्धों में सबसे पुराने ‘सरह’ (सरोजवज्र भी नाम है) हैं जिनका काल डॉ विनयतोष भट्टाचार्य्य ने विक्रम संवत् 690 निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं
- अंतस्साधना पर जोर और पंडितो को फटकार-
- पंडिअ सअल सत्त बक्खाणइ। देहहि बुद्ध बसंत न जाणइ।
- अमणागमण ण तेन बिखंडिअ। तोवि णिलज्ज भणइ हउँ पंडिअ।।
- जहि मन पवन ने संचरइ, रवि ससि नाहि पवेस।
- तहिं बट चित्त बिसाम करु, सरेहे कहिअ उवेस।।
- घोर अँधारे चँदमणि जिमि उज्जोअ करेइ।
- परम महासुह एखु कणे दुरिअ अशेष हरेइ।।
- जीवंतह जो नउ जर सो अजरामर होई।
- गुरु उपएसें बिमलमई सो पर घण्णा कोई॥
- दक्षिण मार्ग छोड़कर वाममार्ग-ग्रहण का उपदेश-
- नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। चिअराअ सहाबे मूकल।
- उजु रे उजु छाड़ि मा लेहु रे बंक। निअहि वोहि मा जादु रे रंक।।
- लूहिपा या लूइपा (संवत् 830 के आसपास) के गीतो से कुछ उद्धरण-
- काआ तरुवर पंच -बिडाल। चंचल चीए पइठो काल ।
- दिट करिअ महासुह परिमाण। लूइ भणई गुरु पुंच्छिअ जाण।।
- भाव न होई, अभाव ण जाई। अइस संबोहे को पतिआइ।
- लुइ भणइ बट दुर्लक्ख बिणाण। तिअ धाए बिलसई, उह लागे णा।
- बिरूपा ( संवत 900 के लगभग ) की वारुणी-प्रेरितं अतर्मुख साधना की पद्धति देखिए-
- सहजे थिर करि वारुणी साध। अजरामर होइ दिट कांध।
- दशमि दुआरत चिह्न देखईआ। आइल गराहक अपणे बहिआ।
- चउशठि घडिए देट पसारा। पइठल गराहक नाहिं निसार।
- कण्हपा ( सं. 900 के उपरांत ) की बानी के कुछ खंड नीचे उद्धृत किए जाते हैं-
- एक्क ण किज्जइ मंत्र ण तंत। णिअ धरणी लइ केलि करंत।
- णिअ घर घरणी जाब ण मज्जइ। ताब किं पंचवर्ण बिहरिज्जइ।
- जिमि लोण बिलज्जइ पाण्डिएहि, तिमि घृरिणी लई चित्त।
- समरस जइ तखणे जइ पुषु ते सम नित्त ।।
- वज्रयानियो की योग-तंत्र-साधना से सच्च तथा स्त्रियों का-विशेषतः डोमिनी, रजकी आदि का-अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कण्हपा डोमिनी का आह्वान-गीत इस प्रकार गाते है-
- नगर बाहिरै डोंबी तोहरि कुडिया छइ।
- छोइ जाई सो बार नाड़िया।।
- कापालिक जोगियो से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननंद आदि देती ही रहती थी, पर वे आकर्षित होती ही थीं-जैसे कृष्ण की ओर गोपियों होती थी—
- राग देस मोह लाइअ छार। परम मोख – लवए मुत्तिहार।
- मारिअ सासु नणंद घरे शाली। माअ मारिया, कण्ह, भइल कबाली।।
- थोड़ा घट के भीतर का विहार देखिए—
- नाडि शक्ति दिअ थरिअ खदे। अनंह, डमरू बाजइ’ बीर नादे।
- काण्ड कपाली जी पाठ अचारे। देह नअरी विहरइ एकारे।।
- इसी ढंग का कुक्कुरिपा (सं॰ 900 के उपरांत) का एक गीत लीजिए––
- ससुरी निंद गेल, बहुडी जागअ। कानैट चोर निलका गइ मागअ।
- दिवसइ बहुढी काढ़ई डरे भाअ। राति भइले कामरू जाअ।
- रहस्य-मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी बानी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई विरला ही बूझ सकता है। सिद्ध तांतिपा की अटपटी बानी सुनिए-
- बेंग संसार बाड़हिल जाअ। दुहिल दूध के बेटे समाअ॥
- बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें पाँच ध्यानी बुद्धों और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते है।
- वज्रयान में आकर ‘महासुखवाद’ का प्रवर्तन हुआ।
- प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुखदशा की प्राप्ति मानी गई।
- इसे आनंद-स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए।
- निर्वाण के तीन अवयव ठहराए गए––शून्य, विज्ञान और महासुख।
- उपनिषद् में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिमाण का अंदाज कराने के लिये उसे सहवास-सुख से सौगुना कहा था पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास-सुख के समान बताया गया।
- शक्तियों सहित देवताओं के ‘युगनद्ध’ स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियों सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगीं, जो कहीं कही अब भी मिलती हैं।
- रहस्य या गुह्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई और ‘गुह्य समाज’ या ‘श्री समाज’ स्थान स्थान पर होने लगे। ऊँचे नीचे कई वर्षों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक बीभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे।
- सिद्धि प्राप्त करने के लिये किसी स्त्री का (जिसे शक्ति, यौगिनी या महामुद्रा कहते थे) योग या सेवन आवश्यक था।
- इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय देश के पूरबी भागों में (बिहार, बंगाल और उड़ीसा में) धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला था।
- रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी बानियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे-
- काआ तरुअर पंच बिड़ाल
- पंच बिड़ाल- बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबद्ध-आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह।
- ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही पांच संख्या निर्गुण धारा के संतो और हिंदी के सूफी कवियों ने ली।
- हिदू शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या 6 हैं ।
- गंगा जउँना माझे बहइ रे नाई ।
- ( इला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा ) इसी से वे अपनी बानियों की भाषा को “संध्याभाषा” कहते थे ।
- ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धो द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे।
- जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानो पर ले हटाकर अंतर्मुख साधनोवाले योगियो पर जमाने का प्रयत्न ‘सरह’ के इस वचन घट में ही बुद्ध है। यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज कहता है कि “मै पंडित हूँ” में स्पष्ट झलकता है।
- यहीं पर यह समझ रखना चाहिए कि योगमार्गी बौद्वो ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी-
- अत्यात्मवेद्यो भगवान् उपमावर्जितः प्रभुः ।।
- सर्वगः सर्वव्यापी च कर्ता हत्त जगत्पतिः ।।
- श्रीमान् वजसत्त्वोऽसौ व्यक्तभाव-प्रकाशक ।।
- -व्यक्त भावानुगत तत्त्वसिद्धि
- (दारिकपा की शिष्या सहजयोगिनी चिता कृत )
- इसी प्रकार जहाँ रवि, शशि, पवन आदि की गति नहीं वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा, ऋजु’ ( सीधे, दक्षिण ) मार्ग छोडकर ‘बंक’ (टेढ़ा, वाम ) मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है।
- सिद्ध कण्हपा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा ?’
- वज्रयान में ‘महासुह’ ( महासुख ) वह दशा बतलाई गई है जिसमे साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिये ‘युगनद्ध’ ( स्त्री-पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा ) की भावना की गई।
- कण्हपा का यह वचन कि “जिमि लौण बिलिज्जइ पाणिएहि तिमि घरणी लई चित्त”, इसी सिद्धांत का द्योतक है।
- कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल, कापालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, ‘गुह्य’ और ‘रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता हैं, वज्रयान इसका प्रमाण है।