“यह कभी हो ही नहीं सकता, देविन्दरलालजी!”
रफ़ीकुद्दीन वकील की वाणी में आग्रह था, चेहरे पर आग्रह के साथ चिन्ता और कुछ व्यथा का भाव। उन्होंने फिर दुहराया, “यह कभी नहीं हो सकता देविन्दरलालजी!”
देविन्दरलालजी ने उनके इस आग्रह को जैसे कबूलते हुए, पर अपनी लाचारी जताते हुए कहा, “सब लोग चले गये। आपसे मुझे कोई डर नहीं, बल्कि आपका तो सहारा है, लेकिन आप जानते हैं, जब एक बार लोगों को डर जकड़ लेता है, और भगदड़ पड़ जाती है, तब फिजा ही कुछ और हो जाती है, हर कोई हर किसी को शुबहे की नज़र से देखता है, और खामखाह दुश्मन हो जाता है। आप तो मुहल्ले के सरवरा हैं, पर बाहर से आने-जाने वालों का क्या ठिकाणा है? आप तो देख ही रहे है, कैसी-कैसी वारदातें हो रही हैं-”
रफ़ीकुद्दीन ने बात काटते हुए कहा, “नहीं साहब, हमारी नाक कट जाएगी! कोई बात है भला कि आप घर-बार छोड़कर अपने ही शहर में पनाहगर्जी हो जाएँ? हम तो आपको जाने न देंगे -बल्कि ज़बरदस्ती रोक लेंगे। मैं तो इसे मेजारिटी फ़र्ज मानता हूँ कि वह माइनारिटी की हिफ़ाज़त करे और उन्हें घर छोड़-छोड़कर भागने न दे। हम पड़ोसी की हिफाज़त न कर सके तो मुल्क की हिफ़ाजत क्या खाक करेंगे! और मुझे पूरा यकीन है कि बाहर की तो खैर बात ही क्या, पंजाब में ही कोई हिन्दू भी, जहाँ उनकी बहुतायत है, ऐसा ही सोच और कर रहे होंगे। आप न जाइए, न जाइए। आपकी हिफ़ाजत की ज़िम्मेदारी मेरे सिर, बस!”
देविन्दरलाल के पड़ोस के हिन्दू परिवार धीरे-धीरे एक-एक करके खिसक गये थे। होता यह कि दोपहर-शाम जब कभी साक्षात् होता, देविन्दरलाल पूछते, “कहो लालजी (या बाऊजी या पंडज्जी) क्या सलाह बणायी है आपने?” और वे उत्तर देते, “जी, सलाह क्या बणाजी है, यहीं रह रहे हैं, देखी जाएगी…” पर शाम को या अगले दिन सवेरे देविन्दरलाल देखते कि वे चुपचाप जरूरी सामान लेकर कहीं खिसक गये हैं, कोई लाहौर से बाहर, कोई लाहौर में ही हिन्दुओं के मुहल्ले में। और अन्त में यह परिस्थिति आ गयी थी कि अब उनके दाहिनी ओर चार मकान खाली छोड़कर एक मुसलमान गूजर का अहाता पड़ता था, जिसमें एक ओर गूजर की भैंसे और दूसरी ओर कई छोटे-मोटे मुसलमान कारीगर रहते थे। बायीं ओर भी देविन्दर और रफ़ीकुद्दीन के मकानों के बीच के मकान खाली थे और रफ़ीकुद्दीन के मकान के बाद मोजंग का अड्डा पड़ता था, जिसके बाद तो विशुद्ध मुसलमान बस्ती थी। देविन्दरलाल और रफ़ीकुद्दीन में पुरानी दोस्ती थी, और एक-एक आदमी के जाने पर उनमें चर्चा होती थी। अन्त में जब एक दिन देविन्दरलाल ने जताया कि वह भी चले जाने की बात पर विचार कर रहे हैं तब रफ़ीकुद्दीन को धक्का लगा और उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, “देविन्दरलालजी, आप भी!”
रफ़ीकुद्दीन का आश्वासन पाकर देविन्दरलाल रह गये। तब यह तय हुआ कि अगर खुदा न करे, कोई खतरे की बात हुई भी, तो रफ़ीकुद्दीन उन्हें पहले ही खबर कर देंगे और हिफ़ाजत का इन्तज़ाम भी कर देंगे – चाहे जैसे हो। देविन्दरलाल की स्त्री तो कुछ दिन पहले की जालंधर मायके गयी हुई थी, उसे लिख दिया गया कि अभी न आये, वहीं रहे। रह गये देविन्दर और उनका पहाड़िया नौकर सन्तू।
किन्तु यह व्यवस्था बहुत दिन नहीं चली। चौथे ही दिन सवेरे उठकर उन्होंने देखा, सन्तू भाग गया है। अपने हाथों चाय बनाकर उन्होंने पी, धोने को बर्तन उठा रहे थे कि रफ़ीकुद्दीन ने आकर खबर दी, सारे शहर में मारकाट हो रही है और थोड़ी देर में मोजंग में भी हत्यारों के गिरोह बँध-बँधकर निकलेंगे। कहीं जाने का समय नहीं है, देविन्दरलाल अपना ज़रूरी और कीमती सामान ले लें और उनके साथ उनके घर चले चलें। यह बला टल जाये तो फिर लौट आएँगे-
‘क़ीमती’ सामना कुछ था नहीं। गहना-छन्ना सब स्त्री के साथ जालंधर चला गया था, रुपया थोड़ा-बहुत बैंक में था; और ज्यादा फैलाव कुछ उन्होंने किया नहीं था। यों गृहस्थ को अपनी गिरस्ती की हर चीज़ कीमती मालूम होती है – देविन्दर लाल घंटे-भर बाद ट्रंक-बिस्तर के साथ रफ़ीकुद्दीन के यहाँ जा पहुँचे।
तीसरे पहर उन्होंने देखा, हुल्लड़ मोज़ंग में आ पहुँचा है। शाम होते-होते उनकी निर्निमेष आँखों के सामने ही उनके घर का ताला तोड़ा गया और जो कुछ था, लुट गया। रात को जहाँ-तहाँ लपटें उठने लगीं, और भादों की उमस धुआँ खाकर और भी गलाघोंटू हो गयी-
रफ़ीकुद्दीन भी आँखों में परायज लिए चुपचाप देखते रहे। केवल एक बार उन्होंने कहा, “यह दिन भी था देखने को – और आज़ादी के नाम पर ! या अल्लाह!
लेकिन खुदा जिसे घर से निकलता है, उसे फिर गली में भी पनाह नहीं देता।
देविन्दरलाल घर से बाहर तो निकल ही न सकते, रफ़ीकुद्दीन ही आते-जाते। काम करने का तो वातावरण ही नहीं था, वे घूम-घाम आते, बाज़ार कर आते। और शहर की खबर ले आते, देविन्दर को सुनाते और फिर दोनों बहुत देर तक देश के भविष्य पर आलोचना किया करते। देविन्दर ने पहले तो लक्ष्य नहीं किया लेकिन बाद में पहचानने लगा कि रफ़ीकुद्दीन की बातों में कुछ चिन्ता का, और कुछ एक और पीड़ा का भी स्वर है जिसे वह नाम नहीं दे सकता – थकान? उदासी? विरक्ति? पराजय? न जाने-
शहर तो वीरान हो गया था। जहाँ-तहाँ लाशें सड़ने लगीं; घर लुट चुके थे और अब जल रहे थे। शहर के एक नामी डॉक्टर के पास कुछ प्रतिष्ठित लोग गये थे यह प्रार्थना लेकर कि वे मुहल्लों में जावें; उनकी सब लोग इज्ज़त करते हैं, इसलिए उनके समझाने का असर होगा और मरीज़ भी वे देख सकेंगे। वे दो मुसलमान नेताओं के साथ निकले। दो-तीन मुहल्ले घूमकर मुसलमानों की बस्ती में एक मरीज़ को देखने के लिए स्टेथस्कोप निकालकर मरीज पर झुके थे कि मरीज के ही एक रिश्तेदार ने पीठ में छुरा भोंक दिया…
हिन्दू मुहल्ले में रेलवे के एक कर्मचारी ने बहुत-से निराश्रितों को अपने घर में जगह दी थी जिनके घर-बार सब लुट चुके थे। पुलिस को उसने खबर दी थी कि वे निराश्रित उसके घर टिके हैं, हो सके तो उनके घरों और माल की हिफ़ाजत की जाए। पुलिस ने आकर शरणागतों के साथ उसे और उसके घर की स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया और ले गयी! पीछे घर पर हमला हुआ, लूट हुई और घर में आग लगा दी गयी। तीन दिन बाद उसे और उसके परिवार को थाने से छोड़ा गया और हिफ़ाजत के लिए हथियारबन्द पुलिस के दो सिपाही साथ किये गये। थाने से पचास क़दम के फ़ासले पर पुलिसवालों ने अचानक बन्दूक उठाकर उस पर और उसके परिवार पर गोली चलाई। वह और तीन स्त्रियाँ मारी गयीं। उसकी माँ और स्त्री घायल होकर गिर गयीं और सड़क पर पड़ी रहीं-
विषाक्त वातावरण, द्वेष और घृणा की चाबुक से तड़फड़ाते हुए हिंसा के घोड़े, विष फैलाने को सम्प्रदाओं को अपने संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकरशाही! देविन्दरलाल को अचानक लगता कि वह और रफ़ीकुद्दीन ही गलत हैं जो कि बैठे हुए हैं जबकि सब-कुछ भड़क रहा है, उफन रहा है, झुलस और जल रहा है-और वे लक्ष्य करते कि वह अस्पष्ट स्वर, जो वे रफ़ीकुद्दीन की बातों में पाते थे, धीरे-धीरे कुछ स्पष्ट होता जाता है – एक लज्जित-सी रुखाई का स्वर-
हिन्दुस्तान-पाकिस्तान की अनुमानित सीमा के पास एक गाँव में कई सौ मुसलमानों ने सिक्खों के गाँव में शरण पायी। अन्त में जब आस-पास के गाँव के और अमृतसर शहर के लोगों के दबाव ने उस गाँव में उनके लिए फिर आसन्न संकट की स्थिति पैदा कर दी, तब गाँव के लोगों ने अपने मेहमानों को अमृतसर स्टेशन पहुँचाने का निश्चय किया जहाँ से वे सुरक्षित मुसलमान इलाके में जा सकें, और दो-ढाई सौ आदमी किरपानें निकालकर उन्हें घेर में लेकर स्टेशन पहुँचा आये – किसी को कोई क्षति नहीं पहुँची-
घटना सुनकर रफ़ीकुद्दीन ने कहा, “आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इनसान को झुकना ही पड़ता है। यहाँ तो पूरा गाँव था, फिर भी उन्हें हारना पड़ा। लेकिन आखिर तक उन्होंने निबाहा, इसकी दाद देनी चाहिए। उन्हें पहुँचा आये-”
देविन्दरलाल ने हामी भरी। लेकिन साहस पहला वाक्य उनके स्मृति-पटल पर उभर आया-”आखिर तो लाचारी होती है – अकेले इनसान को झुकना ही पड़ता है!”
उन्होंने एक तीखी नजर से रफ़ीकुद्दीन की ओर देखा, पर वे कुछ बोले नहीं।
अपराह्न में छःसात आदमी रफ़ीकुद्दीन से मिलने आये। रफ़ीकुद्दीन ने उन्हें अपनी बैठक में ले जाकर दरवाज़े बन्द कर लिए। डेढ़-दो घंटे तक बातें हुई। सारी बात प्रायः धीरे-धीरे ही हुई, बीच-बीच में कोई स्वर ऊँचा उठ जाता और एक-आध शब्द देविन्दरलाल के कान में पड़ जाता -‘बेवकूफ़ी’, ‘गद्दारी’, ‘इस्लाम’ – वाक्यों को पूरा करने की कोशिश उन्होंने आयासपूर्वक नहीं की। दो घंटे बाद जब उनको विदा करके रफ़ीकुद्दीन बैठक से निकल कर आये, तब भी उनसे लपककर पूछने की स्वाभाविक प्रेरणा को उन्होंने दबाया। पर जब रफ़ीकुद्दीन उनकी ओर न देखकर खिंचा हुआ चेहरा झुकाये उनकी बगल से निकलकर बिना एक शब्द कहे भीतर जाने लगे तब उनसे न रहा गया और उन्होंने आग्रह के स्वर में पूछा, “क्या बात है, रफ़ीक साहब, खैर तो है?”
रफ़ीकुद्दीन ने मुँह उठाकर एक बार उनकी ओर देखा, बोले नहीं। फिर आँख झुका लीं।
अब देविन्दरलाल ने कहा, “मैं समझता हूँ कि मेरी वजह से आपको ज़लील होना पड़ा रहा है। और खतरा उठाना पड़ रहा है सो अलग। लेकिन आप मुझे जाने दीजिये। मेरे लिए आप जोखिम में न पड़ें। आपने जो कुछ किया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका एहसान-”
रफ़ीकुद्दीन ने दोनों हाथ देविन्दरलाल के कन्धों पर रख दिये। कहा, “देविन्दरलाल जी!” उनकी साँस तेज़ चलने लगी। फिर वह सहसा भीतर चले गये।
लेकिन खाने के वक़्त देविन्दरलाल ने फिर सवाल उठाया। बोले, “आप खुशी से न जाने देंगे तो मैं चुपचाप खिसक जाऊँगा। आप सच-सच बतलाइए, आपसे उन्होंने कहा क्या?”
“धमकियाँ देते रहे और क्या?”
“फिर भी, क्या धमकी आखिर…”
“धमकी को भी ‘क्या होती है क्या? उन्हें शिकार चाहिए – हल्ला करने न मिलेगा तो आग लगा कर लेंगे।”
“ऐसा! तभी तो मैं कहता हूँ, मैं चला। मैं इस वक्त अकेला आदमी हूँ, कहीं निकल ही जाऊँगा, आप घर-बार वाले आदमी – ये लोग तो सब तबाह कर डालने पर तुले हैं।”
“गुंडे हैं बिलकुल!”
“मैं आज की चला जाऊँगा…”
“यह कैसे हो सकता है? आखिर आपको चले जाने से हमीं ने रोका था, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है…”
“आपने भला चाहकर ही रोका था – उसके आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है…”
“आप जावेंगे कहाँ…”
“देखा जाएगा…”
“नहीं, यह नामुमकिन बात है।”
किन्तु बहस के बाद तय हुआ कि देविन्दरलाल वहाँ से टल जाएँगे। रफ़ीकुद्दीन और कहीं पड़ोस में उनके एक और मुसलमान दोस्त के यहाँ छिपकर रहने का प्रबन्ध कर देंगे – वहाँ तकलीफ़ तो होगी पर खतरा नहीं होगा, क्योंकि देविन्दरलाल घर में रहेंगे। वहाँ पर रहकर जान की हिफ़ाज़त तो रहेगी, तब तक कुछ और उपाय सोचा जाएगा निकलने का…
देविन्दरलाल शेख अताउल्लाह के अहाते के अन्दर पिछली तरफ पेड़ों के झुरमुट की आड़ में बनी हुई एक गैराज में पहुँच गये। ठीक गैराज में तो नहीं, गैराज की बगल में एक कोठरी थी जिसके सामने दीवारों से घिरा एक छोटा-सा आँगन था। पहले शायद यह ड्राइवर के रहने के काम आती हो। कोठरी में ठीक सामने और गैराज की तरफ के किवाड़ों को छोड़कर खिड़की वगैरह नहीं थी। एक तरफ एक खाट पड़ी थी, आले में एक लोटा। फर्श कच्चा, मगर लिपा हुआ। गैराज के बाहर लोह की चादर का मजबूत फाटक था, जिसमें ताला पड़ा था। फाटक के अन्दर ही कच्चे फर्श में एक गढ़ा-सा खुदा हुआ था जिसकी एक ओर चूना-मिली मिट्टी का ढ़ेर और एक मिट्टी का लोटा देखकर गढ़े का उपयेाग समझते देर न लगी।
देविन्दरलाल का ट्रंक और बिस्तर जब कोठरी के कोने में रख दिया गया और बाहर आँगन का फाटक बन्द करके उसमें भी ताला लगा दिया गया, तब थोड़ी देर वे हतबुद्धि खड़े रहे। यह है आज़ादी! पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी, वे आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे; अब अपने ही भाई अपनों को तनहाई क़ैद रहे हैं क्योंकि वे आज़ादी के लिए ही लड़ाई रोकना चाहते हैं! फिर मानव प्राणी का स्वाभाविक वस्तुवाद जागा, और उन्होंने गैराज-कोठरी-आँगन का निरीक्षण इस दृष्टि से आरम्भ किया किया कि क्या-क्या सुविधाएँ वे अपने लिए कर सकते हैं।
गैराज – ठीक है; थोड़ी-सी दुर्गन्ध होगी, ज्यादा नहीं; बीच का किवाड़ बन्द कामचलाऊ रोशनी आँगन से प्रतिबिम्बित होकर आ जाती है, क्योंकि आँगन की एक ओर सामने की मकान की कोने वाली बत्ती से रोशनी पड़ती है। बल्कि आँगन में इस जगह खड़े होकर शायद कुछ पढ़ा भी जा सके। लेकिन पढ़ने को है ही कुछ नहीं, यह तो ध्यान ही न रहा था!
देविन्दरलाल फिर ठिठक गये। सरकारी क़ैद में तो गा-चिल्ला भी सकते हैं, यहाँ तो चुप रहना होगा!
उन्हें याद आया, उन्होंने पढ़ा है, जेल में लोग चिड़िया, कबूतर, गिलहरी, बिल्ली आदि से दोस्ती करके अकेलापन दूर करते हैं; यह भी न होती तो कोठरी में मकड़ी-चीटी आदि का अध्ययन करके… उन्होंने एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई। मच्छरों से भी बन्धु-भाव हो सकता है, यह उनका मन किसी तरह नहीं स्वीकार कर पाया।
वे आँगन में खड़े होकर आकाश देखने लगे। आजाद देश का आकाश! और नीचे से, अभ्यर्थना में – जलते हुए घरों का धुआँ! धूपेन धापयामः। लाल चन्दन-रक्त चन्दन…
अचानक इन्होंने आँगन की दीवार पर एक छाया देखी – एक बिलार! उन्होंने बुलाया, “आओ, आओ!” पर वह वहीं बैठा स्थिर दृष्टि से ताकता रहा।
जहाँ बिलार आता है, वहाँ अकेलापन नहीं है। देविन्दरलाल ने कोठरी में जाकर बिस्तरा बिछाया और थोड़ी देर में निर्द्वन्द्व भाव से सो गये।
दिन छिपे के वक़्त केवल एक बार खाना खाता था। यों वे दो वक़्त के लिए काफ़ी होता था। उसी समय कोठरी और गैराज के लोटे भर दिए जाते थे। लाता था एक जवान लड़का, जो स्पष्ट ही नौकर नहीं था; देविन्दरलाल ने अनुमान किया कि शेख साहब का लड़का होगा। वह बोलता बिलकुल नहीं था। देविन्दरलाल ने पहले दिन पूछा था कि शहर का क्या हाल है तो उसने एक अजनबी दृष्टि से इन्हें देख लिया था। फिर पूछा कि अभी अमन हुआ है या नहीं? तो उसने नकारात्मक सिर हिला दिया था। और सब खैरियत ? तो फिर सिर हिलाया था – हाँ।
देविन्दरलाल चाहते तो खाना दूसरे वक्त के लिए रख सकते थे; पर एक बार आता तो एक बार ही खा लेना चाहिए, यह सोचकर वे डरकर खा लेते थे और बाक़ी बिलार को दे देते थे। बिलार खूब हिल गया था, आकर गोद में बैठ जाता और खाता रहता, फिर हड्डी-बड्डी लेकर आँगन के कोने में बैठकर चबाता रहता या ऊब जाता तो देविन्दरलाल के पास आकर घुरघुराने लगता।
इस तरह शाम कट जाती थी, रात घनी हो जाती थी। तब वे सो जाते थे। सुबह उठकर आँगन में कुछ वरज़िश कर लेते थे कि शरीर ठीक रहे; बाक़ी दिन कोठरी में बैठे कभी कंकड़ों से खेलते, कभी आँगन की दीवार पर बैठनेवाली गोरैया देखते, कभी दूर से कबूतर से गुटरगूँ सुनते-और कभी सामने के कोने से शेखजी के घर के लोगों की बातचीत भी सुन पड़ती। अलग-अलग आवाज़ें वे पहचानने लगे थे, और तीन-चार दिन में ही वे घर के भीतर के जीवन और व्यक्तियों से परिचित हो गये थे। एक भारी – ज़नाना आवाज़ थी – शेख साहब की बीवी की; एक और तीखी ज़नाना आवाज़ थी जिसके स्वर में वय का खुरदरापन था – घर की कोई और बुजुर्ग स्त्री; एक विनीत युवा स्वर था जो प्रायः पहली आवाज़ की ‘जैबू! जैबूनी!’ पुकार के उत्तर में बोलता था और इसलिए शेख साहब की लड़की ज़ैबुन्निसा का स्वर था। दो मर्दानी आवाज़ें भी सुन पड़ती थीं – एक तो आबिद मियाँ की जो, शेख साहब का लड़का हुआ और जो इसलिए वही लड़का है जो खाना लेकर आता है, और एक बड़ी भारी और चरबी से चिकनी आवाज़ तो शेख साहब की आवाज़ है। इस आवाज़ को देविन्दरलाल सुन तो सकते लेकिन इसकी बात के शब्दाकार कभी पहचान में न आते – दूर से तीखी आवाज़ों के बोल ही स्पष्ट समझ आते हैं।
जैबू की आवाज़ से देविन्दरलाल का लगाव था। घर की युवती लड़की की आवाज़ थी, इस स्वाभाविक आकर्षण से ही नहीं, वह विनीत भी थी। इसलिए। मन ही मन वे जेबुन्निसा के बारे में अपने ऊहापोह का रोमानी खेलबाड़ कहकर अपने को थोड़ा झिझक भी लेते थे, पर अक्सर वे यह भी सोचते थे कि क्या यह आवाज़ भी लोगों में फ़िरकापरस्ती का ज़हर भरती होगी? भर सकती होगी? शेख साहब पुलिस के किसी दफ्तर में शायद हेड क्लर्क हैं। देविन्दरलाल को यहाँ लाते समय रफ़ीकुद्दीन ने यही कहा था कि पुलिसियों का घर तो सुरक्षित होता है;
वह बात ठीक है, लेकिन सुरक्षित होता है इसलिए शायद बहुत-से उपद्रवों की जड़ भी होता है। – ऐसे घर में लोग ज़हर फैलानेवाले हों तो अचम्भा क्या…
लेकिन खाते वक्त भी वे सोचते, खाने में कौन-सी चीज़ किस हाथ की बनी होगी, परोसा किसने होगा। सुनी बातों से वे जानते थे कि पकाने में बड़ा हिस्सा तो उस तीखी खुरदरी आवाज़वाली स्त्री का रहता था, पर परोसना शायद जेबुन्निसा के ही ज़िम्मे था। और यही सब सोचते-सोचते देविन्दरलाल खाना खाते और कुछ ज्यादा ही खा लेते थे…
खाने में बड़ी-बड़ी मुसलमानों रोटी के बजाय छोटे-छोटे हिन्दू फुल्के देखकर देविन्दरलाल के जीवन की एकरसता में थोड़ा-सा परिवर्तन आया। मांस तो था, लेकिन आज रबड़ी भी थी जबकि पीछे मीठे के नाम पर एक-आध बार शाह टुकड़ा और एक बार फिरनी आयी थी। आबिद जब खाना रखकर चला गया, तब देविन्दरलाल क्षण-भर उसे रखते रहे। उनकी उँगलियाँ फुल्कों से खेलने-सी लगीं – उन्होंने एकाध को उठाकर फिर रख दिया; पल-भर के लिए अपने घर का दृश्य उनकी आँखों के आगे दौड़ गया। उन्होंने फिर दो-एक फुल्के उठाये और फिर रख दिये।
हठात् वे चौंके।
तीन-एक फुल्कों की तह के बीच में काग़ज की एक पुड़िया-सी पड़ी थी।
देविन्दरलाल ने पुड़िया खोली।
पुड़िया में कुछ नहीं था।
देविन्दरलाल उसे फिर गोल करके फेंक देनेवाले ही थे हाथ ठिठक गया। उन्होंने कोठरी से आँगन में जाकर कोने में पंजों पर खड़े होकर बाहर की रोशनी में पुर्जा देखा, उस पर कुछ लिखा था केवल एक सतर-
“खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा।”
देविन्दरलाल ने कागज़ की चिन्दियाँ कीं। चिन्दियों को मसला। कोठरी से गैराज में जाकर उसे गड्ढे में डाल दिया। फिर आँगन में लौट आये और टहलने लगे।
मस्तिष्क ने कुछ नहीं कहा। सन्न रहा। केवल एक नाम उसके भीतर खोया-सा चक्कर काटता रहा, जैबू… जैबू जैबू…
थोड़ी देर बाद वह फिर खाने के पास जाकर खड़े हो गये।
यह उनका खाना है – देविन्दरलाल का। मित्र के नहीं, तो मित्र के मित्र के यहाँ से आया है। और उनके मेज़बान के, उनके आश्रयदाता के।
जैबू के।
जैबू के पिता के।
कुत्ता यहाँ कहाँ है?
देविन्दरलाल टहलने लगे।
आँगन की दीवार पर छाया सरकी। बिलार बैठा था।
देविन्दरलाल ने बुलाया। वह लपककर कन्धे पर आ रहा। देविन्दरलाल ने उसे गोद में लिया और पीठ सहलाने लगे। वह घुरघुराने लगा। देविन्दरलाल कोठरी में गये। थोड़ी देर बिलार को पुकारते रहे, फिर धीरे-धीरे बोले, “देखो, बेटा, तुम मेरे मेहमान, मैं शेख साहब का, है न? वे मेरे साथ जो करना चाहते हैं, वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। चाहता नहीं हूँ, पर करने जा रहा हूँ। वे भी चाहते हैं कि नहीं, पता नहीं, यही तो जानना है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ वह करना चाहता हूँ जो मेरे साथ वे पता नहीं चाहते हैं कि नहीं… नहीं, सब बात गड़बड़ हो गयी। “अच्छा, रोज़ मेरी जूठन तुम खाते हो, आज तुम्हारी मैं खाऊँगा। हाँ, यह ठीक है। लो, खाओ…”
बिलार ने मांस खाया। हड्डी झपटना चाहता था, पर देविन्दरलाल ने उसे गोदी में लिये-लिये ही रबड़ी खिलाई – वह सब चाट गया। देविन्दरलाल उसे गोदी में लिये सहलाते रहे।
जानवरों में तो सहज ज्ञान होता है खाद्य-अखाद्य का, नहीं तो वे बचते कैसे? सब जानवरों में होता है, और बिल्ली तो जानवरों में शायद सबसे अधिक ज्ञान के सहारे जीनेवाली है, तभी तो कुत्ते की तरह पलती नहीं… बिल्ली जो खा ले वह सर्वथा खाद्य है – यों बिल्ली बड़ी मछली खा ले जिसे इनसान न खाये वह और बात है…
सहसा बिलार ज़ोर से गुस्से से चीखा और उछलकर गोद से बाह जा कूदा, चीखता – गुर्राता-सा कूदकर दीवार पर चढ़ा और गैराज़ की छत पर जा पहुँचा। वहाँ से थोड़ी देर तक उसके कानों में अपने-आपसे ही लड़ने की आवाज़ आती रही। फिर धीरे-धीरे गुस्से का स्वर दर्द के स्वर में परिणत हुआ, फिर एक करुण रिरियाहट में, एक दुर्बल चीख में, एक बुझती हुई-सी कराह में, फिर एक सहसा चुप हो जाने वाली लम्बी साँस में-
मर गया…
देविन्दरलाल फिर खाने को देखने लगे। वह कुछ साफ़-साफ़ दीखता हो सो नहीं; पर देविन्दरलाल जी की आँखें निःस्पन्द उसे देखती रहीं।
आज़ादी भाईचारा। देश-राष्ट्र…
एक ने कहा कि हम ज़ोर करके रखेंगे और रक्षा करेंगे, पर घर से निकाल दिया। दूसरे ने आश्रय दिया, और विष दिया।
और साथ में चेतावनी की विष दिया जा रहा है।
देविन्दरलाल का मन ग्लानि से उमड़ आया। इस धक्के को राजनीति की भुरभुरी रेत की दीवार के सहारे नहीं दर्शन के सहारे ही झेला जा सकता था।
देविन्दरलाल ने जाना कि दुनिया में खतरा बुरे की ताक़त के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। भलाई की साहसहीनता ही बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है।
उन्होंने खाना उठाकर बाहर आँगन में रख दिया। दो घूँट पानी पिया। फिर टहलने लगे।
तानिक देर बाद उन्होंने आकर ट्रंक खोला। एक बार सरसरी दृष्टि से सब चीज़ो को देखा, फिर ऊपर के खाने में दो-एक काग़ज, दो-एक फोटो, एक सेविंग बैंक की पास-बुक और एक बड़ा-सा लिफ़ाफ़ा निकालकर, एक काले शेरवानी-नुमा कोट की जेब में रखकर कोट पहन लिया। आँगन में आकर एक क्षण-भर कान लगाकर सुना।
फिर वे आँगन की दीवार पर चढ़कर बाहर फाँद गये और बाहर सड़क पर निकल आए – वे स्वयं नहीं जान सके कि कैसे!
इसके बाद की घटना, घटना नहीं है। घटनाएँ सब अधूरी होती हैं। पूरी तो कहानी होती है। कहानी की संगति मानवीय तर्क या विवेक या कला या सौन्दर्य-बोध की बनाई हुई संगति मानव पर किसी शक्ति की-कह लीजिए काल या प्रकृति या संयोग या दैव या भगवान की-बनाई हुई संगति है। इसलिए मानव को सहसा नहीं भी दीखती। इसलिए इसके बाद जो कुछ हुआ और जैसे हुआ, वह बताना ज़रूरी नहीं। इतना बताने से काम चल जाएगा कि डेढ़ महीने बाद अपने घर का पता लेने के लिए देविन्दरलाल अपना पता देकर दिल्ली-रेडिया से अपील करवा रहे थे तब एक दिन उन्हें लाहौर की मुहरवाली एक छोटी-सी चिट्ठी मिली थी।
“आप बचकर चले गये, इसके लिए खुदा का लाख-लाख शुक्र है। मैं मनाती हूँ कि रेडियो पर जिनके नाम आपने अपील की है, वे सब सलामती से आपके पास पहुँच जाएँ। अब्बा ने जो किया या करना चाहा, उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ और यह भी याद शायद दिलाती हूँ कि उसकी काट मैंने ही कर दी थी। अहसान नहीं जताती – मेरा कोई अहसान आप पर नहीं है -सिर्फ़ यह इल्तजा करती हूँ कि आपके मुल्क में अक़लियत का कोई मज़लूम हो तो याद कर लीजिएगा।
इसलिए नहीं कि वह मुसलमान है, इसलिए कि आप इनसान हैं। खुदा हाफिज़!”
देविन्दरलाल की स्मृति में शेखउल्लाह की चरबी से चिकनी भारी आवाज़ गूँज गयी, “जैबू! जैबू!” और फिर गैराज की छत पर छटपटाकर धीरे-धीरे शान्त होनेवाली बिलार की वह दर्द-भारी कराह, जो केवल एक लम्बी साँस बनकर चुप हो गयी थी।
उन्होंने चिट्ठी को छोटी-सी गोली बनाकर चुटकी से उड़ा दी।
(इलाहाबाद, 1947)



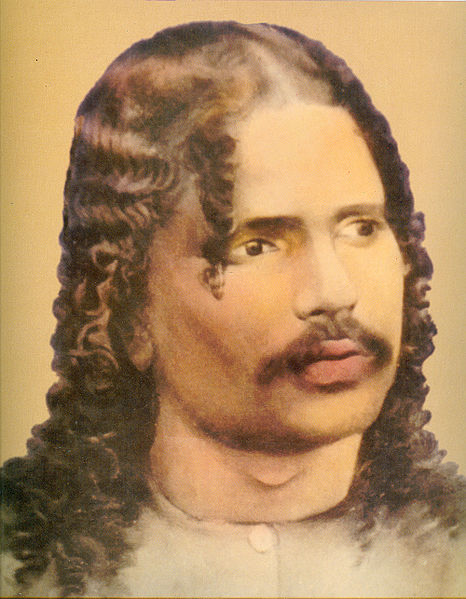


2 responses to “शरणदाता – सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ‘अज्ञेय’”
Kya aap RPSC ke syllabus me lagi kahaniyan uplabdh Kara sakte Hain?
उम्दा